 नारायण दत्त >
नारायण दत्त >
अभावों और असुविधाओं से जूझते हुए अपने व्यक्तित्व को अपने हाथों गढ़ना और जीवन-पथ पर अविचल भाव से आगे बढ़ते जाना आदमी के आत्मबल को सूचित करता है. मेरे मित्रों और सहकर्मियों में श्री गिरिजाशंकर त्रिवेदी आत्मबल के मामले में असंदिग्ध रूप से धनी थे. किशोरावस्था से निकलने के साथ ही पढ़ाई बंद करके जीविकोपार्जन में जुट जाना उनके लिए ज़रूरी हो गया था. परिवार के बड़े बेटे के रूप में अपने कंधों पर आ पड़े कर्तव्यों को उन्होंने धीरता के साथ निभाया. साथ ही अपनी महत्त्वाकांक्षा और उसे पूरा करने के संकल्प को भी उन्होंने जिलाये रखा, जो कि शायद कम आत्मबल वाले व्यक्ति के लिए सम्भव न होता.
कई जगह काम करने के बाद 1960 में वे हमारे सम्पादक श्री सत्यकाम विद्यालंकार के निजी सहायक के रूप में ‘नवनीत’ के स्टाफ में शामिल हुए. उनकी क्षमताओं को देखकर एक-डेढ़ साल बाद उन्हें सम्पादकीय विभाग में स्थान दिया गया. क्रमेण पदवृद्धि पाते हुए अंततः वे सम्पादक के पद पर पहुंचे और दीर्घकाल तक उस पर आसीन रहे. विशेष बात यह भी कि दफ़्तर के कामकाज और पत्नी एवं पांच बच्चों के परिवार के भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी निभाते हुए उन्होंने प्राइवेट विद्यार्थी के तौर पर इंटरमीडिएट, बी.ए. और अंततः एम.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की, जो कि कम आत्मबल वाले व्यक्ति के बूते की बात नहीं थी. स्वभाव से श्री त्रिवेदी स्थिरचित्त थे. काम का बोझ उन्हें कभी उद्विग्न नहीं करता था. वे भरोसेमंद साथी और सहृदय सहकर्मी थे. इन खूबियों ने उन्हें नवनीत-कार्यालय का एक सुदृढ़ स्तम्भ बना दिया था.
साथ ही वे एक सार्वजनिक व्यक्ति भी थे. मुम्बई के हिंदी भाषी जगत में उनका अपना विशिष्ट स्थान था. वे हिंदी कविता के रसिक थे और स्वयं कवि थे. मुम्बई में बचपन से पलने के कारण मराठी और गुजराती अच्छी तरह जानते थे. उनका मित्र-वृंद विशाल था. यह सोचकर दुःख होता है कि दृढ़ काया और नियमित दिनचर्या वाले श्री त्रिवेदी को जीवन के अंतिम दौर में जिगर के कैन्सर से जूझना पड़ा. योग्य चिकित्सकों के इलाज और अच्छी सुश्रुषा के बावजूद 87 वर्ष की उम्र में उनका देहावसान हो गया. उनकी पत्नी श्रीमती विद्यादेवी कुछ वर्ष पहले ही चल बसी थीं.
(जनवरी 2014)
]]> महात्मा गांधी >
महात्मा गांधी >
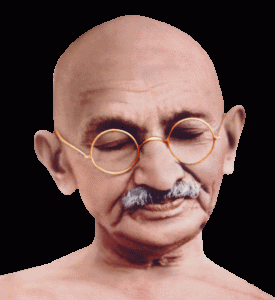 मेरे एक रिश्तेदार के साथ मुझे बीड़ी-सिगरेट पीने का चस्का लगा. हमारे पास पैसे तो होते नहीं थे. हम दोनों में से किसी को यह पता नहीं था कि सिगरेट पीने से कोई फायदा होता है या उसकी गंध में कोई आनंद होता है. लेकिन हमें लगा कि सिगरेट का धुआं उड़ाने में ही असली मज़ा है. मेरे चाचा को सिगरेट पीने की लत थी. उन्हें और दूसरे बुजुर्गों को धुआं उड़ाते देख हमारी भी सिगरेट फूंकने की इच्छा हुई. गांठ में पैसे तो थे नहीं, इसलिए चाचा सिगरेट पीने के बाद जो ठूंठ फेंक देते, हमने उन्हें ही चुरा कर पीना शुरू कर दिया.
मेरे एक रिश्तेदार के साथ मुझे बीड़ी-सिगरेट पीने का चस्का लगा. हमारे पास पैसे तो होते नहीं थे. हम दोनों में से किसी को यह पता नहीं था कि सिगरेट पीने से कोई फायदा होता है या उसकी गंध में कोई आनंद होता है. लेकिन हमें लगा कि सिगरेट का धुआं उड़ाने में ही असली मज़ा है. मेरे चाचा को सिगरेट पीने की लत थी. उन्हें और दूसरे बुजुर्गों को धुआं उड़ाते देख हमारी भी सिगरेट फूंकने की इच्छा हुई. गांठ में पैसे तो थे नहीं, इसलिए चाचा सिगरेट पीने के बाद जो ठूंठ फेंक देते, हमने उन्हें ही चुरा कर पीना शुरू कर दिया.
लेकिन सिगरेट के ये ठूंठ हर समय तो मिल नहीं सकते थे और इनमें से धुआं भी बहुत नहीं निकलता था. इसलिए नौकर की जेब में पड़े पैसों में से एकाध पैसा चुराने की आदत डाली और इन पैसों से हम बीड़ी खरीदने लगे. लेकिन अब सवाल पैदा हुआ कि उसे सम्भाल कर रखें कहां? हम जानते थे कि बुजुर्गों की निगाह के सामने तो हम बीड़ी-सिगरेट पी ही नहीं सकते. जैसे-तैसे दो चार पैसे चुरा कर कुछ हफ्ते काम चलाया. इस बीच पता चला कि एक तरह का पौधा होता है (उसका नाम तो मैं भूल ही गया हूं) जिसके डंठल सिगरेट की तरह जलते हैं और फूंके जा सकते हैं. हमने ऐसे डंठल खोजे और उन्हें सिगरेट की तरह फूंकने लगे.
लेकिन इससे हमें संतोष न हुआ. अपनी पराधीनता हमें अखरने लगी. हमें दुःख इस बात का था कि बड़ों की आज्ञा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते थे. हम ऊब गये और हमने आत्महत्या करने का फैसला कर डाला!
पर आत्माहत्या कैसे करें? ज़हर कौन देगा? हमने सुना कि धतूरे के बीज खाने से मृत्यु हो जाती है. हम जंगल में जा कर धतूरे के बीज ले आये. शाम का समय तय किया. केदारनाथ जी के मंदिर में दीप माला में घी चढ़ाया, भगवान के दर्शन किये और सुनसान जगह की तलाश की. लेकिन ज़हर खाने की हिम्मत न हो. अगर तुरंत मृत्यु न हुई तो क्या होगा? मरने से लाभ क्या? क्यों न पराधनीता ही सह ली जाये? फिर भी दो-चार बीज खाये. अधिक बीज खाने की हिम्मत ही न हुई. हम दोनों ही मौत से डरे और तय किया कि राम जी के मंदिर में दर्शन करके शांत हो जायें और आत्महत्या करने की बात भूल जाएं.
मैं इस बात को समझ पाया कि मन में आत्महत्या का विचार लाना कितना आसान है और सचमुच आत्महत्या करना कितना मुश्किल. इसलिए जब कोई आत्महत्या करने की धमकी देता है तो मुझ पर उसका बहुत कम असर होता है या यह भी कहा जा सकता है कि बिल्कुल भी नहीं होता.
आत्महत्या के इस विचार का नतीजा ये हुआ कि हम दोनों की सिगरेट चुरा कर पीने की और नौकरों की जेब से पैसे चुरा कर सिगरेट फूंकने की आदत जाती रही. बड़े हो कर सिगरेट पीने की कभी इच्छा ही नहीं हुई. मैं हमेशा यही मान कर चलता रहा कि सिगरेट पीने की आदत जंगली, गंदी और नुकसान दायक है. मैं आज तक इस बात को समझ नहीं सका हूं कि पूरी दुनिया में सिगरेट-बीड़ी पीने या धूम्रपान करने का इतना शौक क्यों है? रेलगाड़ी के जिस डिब्बे में सिगरेट पी जाती है, उसमें बैठना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है और धुएं से मेरा दम घुटने लगता है.
सिगरेट के ठूंठ चुराने और इस सिलसिले में नौकर की जेब से पैसे चुराने का दोषी तो मैं हूं ही, एक और चोरी का जो दोष हुआ मुझसे, मैं उसे गगज्यादा गम्भीर मानता हूं. सिगरेट पीने के दोष के समय मेरी उम्र बारह या तेरह बरस की रही होगी. शायद इससे भी कम हो. दूसरी चोरी के समय मेरी उम्र पंद्रह बरस के आसपास थी. यह चोरी मेरे मांसाहारी भाई के सोने के कड़े के एक टुकड़े की थी. उन पर मामूली-सा, लगभग पच्चीस रुपये का कर्ज हो गया था. हम दोनों भाई इस बात को ले कर परेशान थे कि ये कर्ज कैसे चुकाया जाए. मेरे भाई के हाथ में खरे सोने का कड़ा था. उसमें से एक तोला सोना काट लेना मुश्किल न था.
कड़ा कटा. कर्ज चुकाया गया. लेकिन मेरे लिए यह बात सहन करना आसान न था. मैंने तय किया कि आगे से कभी चोरी नहीं करूंगा. मुझे ऐसा भी लगा कि पिताजी के सामने जा कर अपना गुनाह भी कबूल कर लेना चाहिए. लेकिन जुबान ही न खुले. इस बात का डर तो था ही नहीं कि पिताजी पीटेंगे. इस बात की कोई याद नहीं थी कि कभी उन्होंने किसी भाई को पीटा-वीटा हो. लेकिन खुद तो दुःखी होंगे ही ना! शायद सिर फोड़ लें! मैंने यह सोचा कि यह जोखिम उठाते हुए भी अपने दोष को कबूल करना ही होगा. इसके बिना शुद्धि नहीं होगी.
आखिर मैंने तय किया कि एक पत्र लिखकर अपना दोष स्वीकार कर लिया जाए और माफी मांग ली जाए. मैंने पत्र लिख कर उन्हें हाथों-हाथ थमा दिया.
मैंने कांपते हाथों से पत्र पिताजी के हाथ में थमाया. मैं उनके तख्त के सामने बैठ गया.
उन्होंने पत्र पढ़ा. उनकी आंखों से मोती टपकने लगे. पत्र भीग गया. उन्होंने पल भर के लिए आंखें मूंदी, पत्र फाड़ डाला. पत्र पढ़ने के लिए वे उठे थे, वापिस लेट गये.
मैं भी रोया. पिताजी का दुःख समझ सका. यदि मैं चित्रकार होता तो उस पल का सम्पूर्ण चित्र बना सकता था. वह दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने जस का तस झिलमिला रहा है.
मोती की बूंदों के उस प्रेम बाण ने मुझे बेध डाला. मैं शुद्ध हो गया. इस प्रेम को तो वही जान सकता है जिसे इसका अनुभव हुआ हो.
राम की भक्ति का बाण जिसे लगा हो, वही जान सकता है.
मेरे लिए ये अहिंसा का साक्षात पाठ था. उस समय तो मैंने इसमें पिता के प्रेम के अतिरिक्त कुछ न देखा. परंतु आज मैं इसे शुद्ध अहिंसा के नाम से पहचान सकता हूं. ऐसी अहिंसा जब विराट रूप धारण कर लेती है तो उसके स्पर्श से कौन बच सकता है. ऐसी विराट अहिंसा की थाह लेना
असम्भव है.
ऐसी शांत क्षमा पिता के स्वभाव के प्रतिकूल थी. मैं तो ये मानकर चल रहा था कि वे गुस्सा होंगे, कड़वे बोल बोलेंगे, शायद सिर भी फोड़ें, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपार शांति धारण की, मेरे विचार से उसके पीछे अपराध की सरल स्वीकृति थी. जो व्यक्ति अधिकारी के सामने स्वेच्छा से और निष्कपट भाव से अपने दोष को स्वीकार कर लेता है और फिर कभी वैसा अपराध न करने की प्रतिज्ञा करता है तो वह शुद्धतम प्रायश्चित करता है.
मैं जानता हूं कि इस स्वीकृति से पिताजी मेरे बारे में निर्भय बने और मेरे प्रति उनका असीम प्रेम और बढ़ गया
(जनवरी 2014)
]]>
